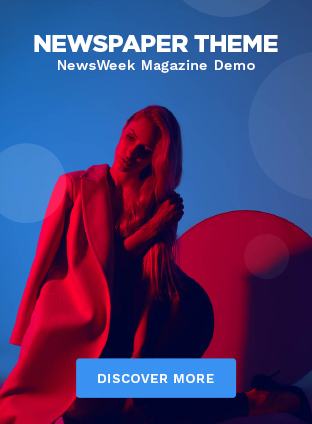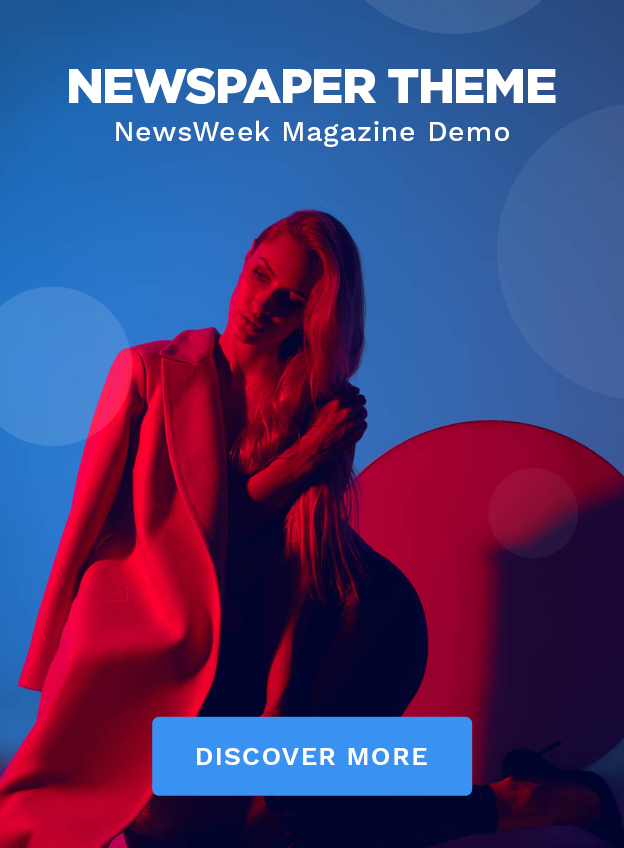चंडीगढ़, 14 जून:
पंजाब राज्य किसान एवं कृषि श्रमिक आयोग की अध्यक्षता में प्रो. डॉ. सुखपाल सिंह के नेतृत्व में पंजाब में जल संकट विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कार्बन डेटिंग, मिट्टी और जल के समस्थानिक (आइसोटोप) अध्ययन और पंजाब में सीपेज (जल रिसाव) से संबंधित एक व्यापक सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययन पर चर्चा की गई। पूर्व बागवानी निदेशक डॉ. गुरकंवल सिंह ने सह-अध्यक्षता की, और आयोजन का प्रबंधन पीएसएफसी के प्रशासनिक अधिकारी-सह-सचिव डॉ. आर.एस. बैंस ने किया।
कार्यशाला के पहले दिन पंजाब की जटिल हाइड्रोजियोलॉजिकल (जल-भूगर्भीय) चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने भूजल प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण अनुसंधानों और सतत समाधानों की प्रस्तुति दी।
पीएयू लुधियाना से डॉ. जे.पी. सिंह और डॉ. समनप्रीत कौर ने भूजल से संबंधित चिंताओं और संभावित समाधानों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। डॉ. कौर ने विशेष रूप से ‘स्मार्ट सबमर्सिबल पंप’ के विकास की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि किसान वास्तविक समय में डेटा प्राप्त कर भूजल का समझदारी से उपयोग कर सकें।
चर्चा में सैलिन क्षेत्रों, भूजल पुनर्भरण की दक्षता और तकनीकों जैसे मुद्दों पर विचार हुआ। उन्होंने बताया कि पीएयू ने वर्षा जल संरक्षण हेतु कई मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। पीने और सिंचाई योग्य जल के प्रदूषण की समस्या भी एक गहरी चिंता का विषय बनी हुई है।
वैज्ञानिकों ने कई अध्ययनों को भी साझा किया, जिनमें पंजाब की जल प्रणालियों का ऐतिहासिक विश्लेषण, भूजल रिचार्ज हेतु परित्यक्त कुओं और गांवों के तालाबों का उपयोग तथा डाइरेक्ट सीडेड राइस (डी एस आर) और पारंपरिक रोपाई वाले धान की खेती के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन शामिल था।
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के मानवविज्ञान और जलविज्ञान विभागों से डॉ. महेश ठाकुर, डॉ. जे.एस. शेखावत, डॉ. प्रकाश तिवारी और डॉ. जुगराज सिंह ने पंजाब में सतत जल प्रबंधन हेतु हाइड्रोजियोलॉजिकल चुनौतियों, शोध निष्कर्षों और प्रस्तावित शोध-आधारित समाधानों पर प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में यूरेनियम और आर्सेनिक जैसे उभरते और खतरनाक जल प्रदूषकों पर केंद्रित रही। उन्होंने पांच जिलों में किए गए अध्ययन की जानकारी साझा की, जिसमें जल और मिट्टी में प्रदूषण की मैपिंग की गई और विशेषकर केंद्रीय पंजाब में गंभीर परिणाम सामने आए। कृषि और औद्योगिक गतिविधियों से मिट्टी में फैलते प्रदूषण पर भी चर्चा की गई। टीम ने जिलेवार स्थानीय मैपिंग, भूजल की गुणवत्ता सूचकांक निर्धारण और सिंचाई उपयुक्तता अध्ययन जैसे और गहन शोध की आवश्यकता पर बल दिया।
दूसरे दिन कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, पंजाब से डॉ. अरुण कुमार, डॉ. संदीप सिंह वालिया, श्री दीपक सेठी और श्रीमती रीतिका ने पंजाब में भूजल की स्थिति पर अपने कार्य प्रस्तुत किए। उनकी रिपोर्ट ने गंभीर स्थिति को उजागर किया कि राज्य के 153 ब्लॉकों में से 115 ब्लॉक अत्यधिक भूजल दोहन के कारण अतिदोहन की श्रेणी में हैं। पंजाब की औसत भूजल निकासी दर 153.86% है, यानी राज्य जितना जल पुनर्भरण करता है, उससे 1.5 गुना अधिक भूजल निकाल रहा है।
भूजल की यह तीव्र कमी लगभग 10 मिलियन एकड़-फुट (एम ए एफ ) की वार्षिक गिरावट के रूप में देखी जा रही है, जो प्राकृतिक पुनर्भरण और दोहन के बीच असंतुलन को दर्शाती है। यह पंजाब की कृषि स्थिरता और जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। इसका मुख्य कारण धान की अत्यधिक जल-आधारित खेती है, जिससे व्यवहारिक विकल्पों और टिकाऊ समाधान हेतु सभी भागीदारों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता सामने आई है।
प्रो. डॉ. सुखपाल सिंह ने आने वाले जल संकट को रोकने हेतु वैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि यद्यपि सभी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, फिर भी एक साझा मंच की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आयोग एक डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जहाँ सभी अनुसंधान संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित और प्रोसेस कर सरकार एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पंजाब की भावी जल नीति बन सके।
डॉ. गुरकंवल सिंह ने शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों के बीच अंतर्विषयी सहयोग पर बल दिया और शोधकर्ताओं से समस्याओं के व्यावहारिक समाधान सुझाने का आग्रह किया।
डॉ. आर.एस. बैंस ने आश्वासन दिया कि पीएसएफसी भविष्य में भी इस तरह के और अध्ययन एवं नीतिगत समर्थन की सुविधा देगा।
यह बैठक पंजाब में सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही, जो दीर्घकालिक कृषि एवं पर्यावरणीय लचीलापन के लिए साक्ष्य-आधारित समाधानों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन शोध निष्कर्षों के आधार पर एक ठोस भविष्य रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे चिरस्थायी कृषि मॉडल विकसित किया जा सके।